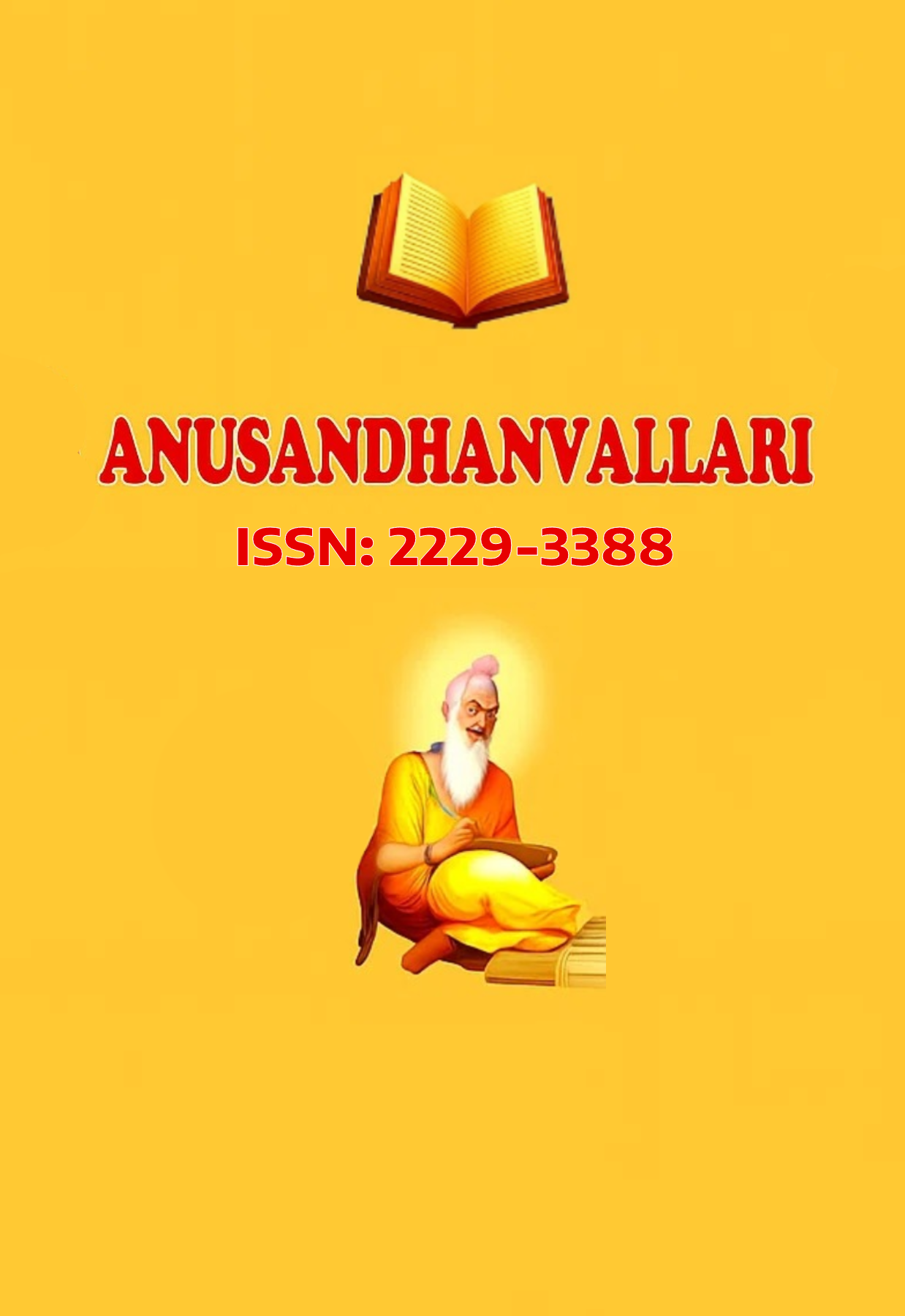पर्यावरण और भारतीय ज्ञान परंपरा
Main Article Content
Abstract
सामान्यतया पर्यावरण का अर्थ प्राकृतिक जगत से लिया जाता है। भूमि, वायुमंडल, नदियां, झीलें, तालाब, समुद्र आदि जल स्रोत एवं जलीय जीव, पहाड़, वन यहां पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के प्राणी आदि सभी प्रकार के जीव पर्यावरण के घटक हैं। इसके अतिरिक्त अंतरिक्ष को भी इसमें हम जोड़ सकते हैं। चिरकाल से इन सभी घटकों के मध्य प्राकृतिक रूप से संतुलन स्थापित है। पर्यावरण हमारे अस्तित्व व विकास दोनों के लिए आवश्यक है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से मनुष्य ने अपने लाभ के लिए प्रकृति का दोहन किया है। यद्यपि प्रारंभ में ऐसा नहीं था परंतु पिछले कुछ दशकों से मनुष्य इस व्यवस्था से छेड़छाड़ करने पर उतारू है और वर्तमान में तो स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि अति संवेदनशील पर्यावरणीय संतुलन के पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने का खतरा भी उत्पन्न हो गया है, परिणामस्वरुप मानव सभ्यता के अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। नष्ट होते पर्यावरण और बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज संपूर्ण विश्व चिंतित है। आजकल पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। 1700 ई. में पृथ्वी का औसत तापमान 15° से. था, जोकि 2050ई.में 16.5° और 2100ई.में 18°- 19° तक या इससे भी कहीं अधिक पहुंच सकता है। तापमान वृद्धि के कारण हिमालय और ध्रुवो तक की हजारों साल से जमी बर्फ पिघलने लगी है, इसके प्रभाव से आने वाले समय में नदियों में समय-समय पर भयंकर बाढ़ आ सकती है, समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय भूमि उसके गर्भ में समा सकती है।वर्तमान समय में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है जो कि पर्यावरण संतुलन के लिए घातक है। पर्यावरण संतुलन के लिए वनों का एक निश्चित प्रतिशत बने रहना आवश्यक है।पश्चिम ने प्रकृति को भोग की वस्तु माना है जबकि भारतीय ज्ञान परंपरा एवं संस्कृति में पर्यावरण और प्रकृति कोई विषय नहीं अपितु जीवन पद्धति है। हमारी भारतीय संस्कृति, प्रकृति प्रेम एवं प्रकृति संरक्षण की चिंतन धारा है। हमारे ऋषि-मुनि इतने उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे कि उन्होंने जड़ चेतन सभी तत्वों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए नियम बनाएं। यही कारण है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में पर्यावरण संरक्षण की बातें कूट-कूट कर भरी पड़ी है।